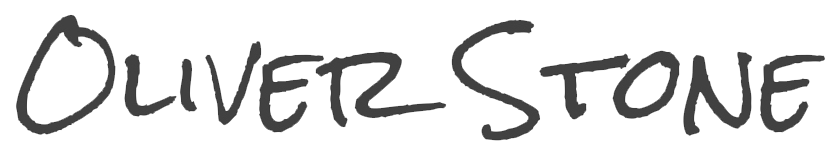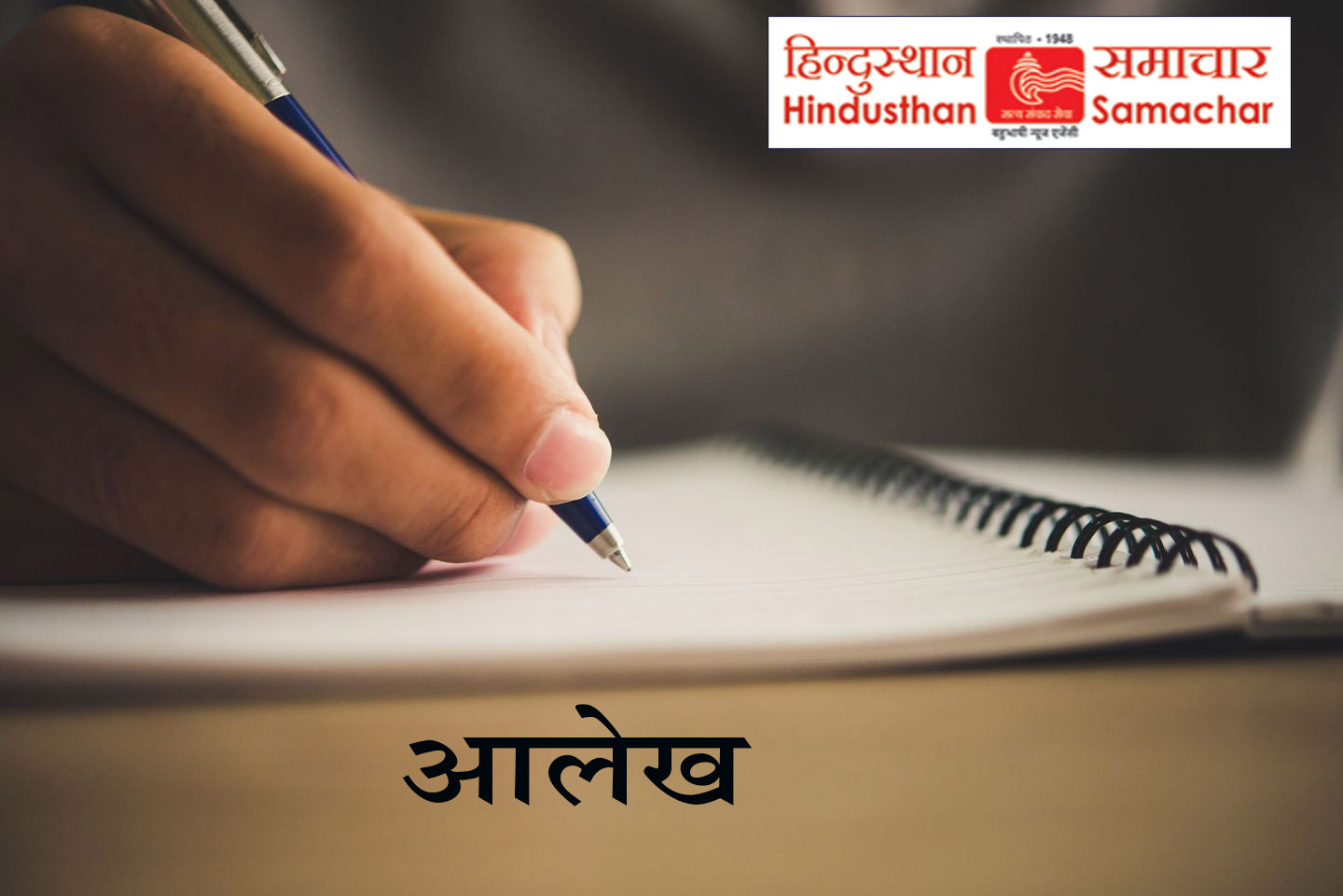Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद् की पुण्यतिथि (03 अप्रैल 1988) पर विशेष
-रमेश शर्मा
डॉक्टर हरिभाऊ वाकणकर की गणना संसार के प्रमुख पुरातत्वविदों में होती है। उन्होंने भारत के विभिन्न वनक्षेत्र के पुरातन जीवन और भोपाल के आसपास लाखों वर्ष पुराने मानव सभ्यता के प्रमाण खोजे। भीमबैठका उन्हीं की खोज है। उनके शोध के बाद विश्व भर के पुरातत्वविद् भारत आये और डाक्टर वाकणकर से मार्गदर्शन लिया। उनका पूरा नाम श्रीविष्णु श्रीधर वाकणकर था लेकिन वे हरिभाऊ वाकणकर के नाम से प्रसिद्ध थे।
उनका जन्म 4 मई 1919 को मध्यप्रदेश के नीमच नगर में हुआ। पिता श्रीधरजी वाकणकर वैदिक विद्वान थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। बड़े भाई लक्ष्मण वाकणकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियर थे। उन्हें सिरेमिक कला में विशेषज्ञता प्राप्त थी। लिपियों के विकास विशेषकर देवनागरी के डिजिटलीकरण में विशेषज्ञ के रूप में उनकी ख्याति थी। हरिभाऊ जी की प्रारंभिक शिक्षा नीमच में ही हुई और उच्च शिक्षा केलिये बनारस गये। पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनके भीतर भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट स्वाभिमान जागृत किया और राष्ट्रीय स्वयं सेवकसंघ से जुड़ने के लिये प्रेरित किया। वे बालवय में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गये थे। हरिभाऊ जी बहुत अध्ययन एवं कल्पनाशील थे, स्मरण शक्ति और स्वत्व वोध विलक्षण था। छात्र जीवन में अपनी कक्षा के साथियों और अन्य मित्रों से परस्पर चर्चा में तर्क सहित वे उन धारणाओं का खंडन करते थे जो विदेशी लेखकों ने भारतीय वाड्मय की गरिमा कम करने के लिये स्थापित की थीं। शिक्षा पूरी कर उन्होंने इसी दिशा में कदम बढ़ाये। उन्होंने भारतीय पुरातन साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया और पुराणों कथाओं से संबंधित विवरणों के सजीव प्रमाण खोजे।अनेक उन तथ्यों को प्रमाणित किया जिन्हें मिथक कहकर नकारा जाता रहा था। इसमें वेद वर्णित सरस्वती नदी का अस्तित्व भी है।
वाकणकर जी ने सरस्वती नदी की खोज के लिये विश्व इतिहास के इस तथ्य को आधार बनाया कि संस्कृतियों के विकास और इतिहास के प्रमाणीकरण में नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वाकणकर जी ने वैदिक साहित्य में वर्णित सरस्वती नदी की खोज आरंभ की। उन्होंने उपग्रह छवि से प्रमाणित किया कि सरस्वती नदी का प्रवाह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरता है। आगे चलकर इस मार्ग के लिये एक परियोजना का गठन हुआ जिसके सलाहकार मंडल कै संयोजक वाकणकर जी बनाये गये। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को भी सरस्वती नदी से जुड़े होने के प्रमाण दिये। पुरातात्विक खोज के लिये उन्होने उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। गंगा और नर्मदा के किनारे, विन्धय एवं सतपुड़ा पर्वत क्षणियों के मैदानों में लाखों वर्ष पुराने मानव सभ्यता के चिन्ह खोजे। पर उन्हें मालवा से बहुत लगाव था। इसलिये उन्होंने नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, कायथा, शाजापुर के साथ भोपाल, रायसेन, विदिशा आदि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया और वनक्षेत्र में पदयात्राएँ कीं। उनके जीवनवृत के अध्ययन से लगता है कि प्रकृति से उन्हें कोई अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त थी। वे पुरातात्विक और खंडित प्रतिमाओं को इतने ध्यान से देखते थे कि लगता था उनसे बातें कर रहे हो। कई बार तो बैठे-बैठे उठकर किसी विशिष्ठ स्थान की ओर चल देते थे अथवा चलती ट्रेन में अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर जंगल में उतर जाते थे और उन्हें वहाँ कुछ न कुछ पुरातात्विक खजाना मिल ही जाता था।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग चालीस किलोमीटर दूर भीमबेटका के प्राचीन शिलाचित्रों की खोज वाकणकरजी ने की थी। भीमबैठका और भोजपुर के आसपास के कुछ चित्र तो लगभग पौने दो लाख वर्ष पुराने प्रमाणित हुये। इन सभी चित्रों का कार्बन-डेटिंग पद्धति से परीक्षण किया गया। इसका सत्यापन अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने किया । इसी शोध के चलते उन्हें 1975 में पद्मश्री अलंकरण मिला।
वाकणकर जी उज्जैन के सिंधिया ओरियंटल इंस्टीट्यूट से जुड़े थे और भारतीय कला मंदिर उनकी साधना स्थली था। वे न केवल पुरातत्वविद् थे अपितु अच्छे चित्रकार भी थे। उन्हें जितनी विशिष्टता पुरातात्विक अनुसंधान में प्राप्त थी वे उतने ही श्रेष्ठ संगठक थे। उनका पूरा जीवन ऋषि परंपपरानुरूप था। उन्होंने अपने शिष्यों की एक विशाल मंडली तैयार की। उनमें श्याम सुंदर सक्सेना, गोमती संकुशल, सचिदा नागदेव , मुजफ्फर कुरैशी, रहीम गुट्टीवाला आदि प्रमुख रहे। अपने शिष्यों की टोली के साथ उन्होंने चंबल और नर्मदा के बीहड़ों की खोज की और इंग्लैड तक यात्रा की। उनका शिष्य मंडल मानों परिवार था, उनके व्यक्तित्व का अंग था। वे सुनते अधिक थे बोलते कम थे। जो बोलते मानों ब्रह्म वाक्य होता। उन्होंने जीवन में कभी विश्राम नहीं किया। उन्होंने निरंतर यात्राएँ कीं, भारत के सभी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थानों के साथ विश्व के अनेक स्थानों की यात्रा इसमें शामिल है। वे कभी भी एक झोला कंधे पर टाँग कर निकल पड़ते थे। जिस प्रकार उनके जीवन का आरंभ भारतीय परंपरा, संस्कृति और श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित करने के अभियान के साथ हुआ था, जीवन का समापन भी कर्मपथ पर हुआ। उन्होंने 4 मई 1988 को सिंगापुर में जीवन की अंतिम श्वाँस ली।
यह उनके व्यक्तित्व और कार्य क्षमता और ऊर्जा की विलक्षण विशेषता थी कि पुरातात्विक अन्वेषण में अपने अतुलीय और अथक कार्य के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्पों में भी उनकी सक्रियता निरन्तर रही। वे 1981 में स्थापित संस्कार भारती के संस्थापक महामंत्री रहे। वनक्षेत्र में अपने शोध कार्य के साथ उन्होने संघ की योजनानुसार सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान कार्य भी किये।
पुरातात्विक अनुसंधान और सामाजिक कार्यों के साथ वाकणकरजी ने सिक्कों और शिलालेखों का संग्रह भी किया। उन्होंने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर अब तक के लगभग 5500 सिक्कों और संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी आदि भाषाओं के लगभग 250 शिलालेखों का संग्रह किया। उनके योगदान की स्मृति को सजीव रखने के लिये संस्कार भारती ने 4 मई 2019 से 3 मई 2020 के बीच उनकी जन्म शताब्दी वर्ष का आयोजन किया था। उनका शरीर भले आज संसार में नहीं है पर उनके अनुसंधान सजीव हैं। वे पुरातात्विक अनुसंधान के मील के पत्थर थे। उनके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी अनुसंधानकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी