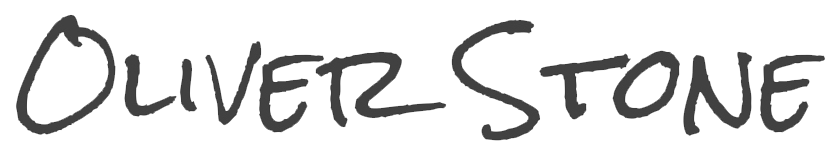Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

गिरीश्वर मिश्र
भारतीय नववर्ष के आरम्भ में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रतिवर्ष राम-जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस उत्सव का व्यापक भारतीय जन समाज की सांस्कृतिक जीवन यात्रा में विशेष महत्त्व है । घट-घट व्यापी अन्तर्यामी परमात्मा को श्रीराम के मानुष रूप में लोकावतरण एक रोमांचकारी अवसर होता है जब हम श्रीराम को अपने जीवन में आसपास पाने की लालसा लिए रामनवमी मनाते हैं। यह मानवीय चेतना के ऊर्ध्वमुखी परिष्कार का एक विलक्षण सोपान बन जाता है। जैसा कि सर्वविदित है प्रभु श्रीराम की मनुष्य लीला एक ऐसे बड़े वितान पर आयोजित है जिसमें कोई सीधी रेखा नहीं है। हाँ, अप्रत्याशित मोड़ जरूर हैं जो उत्सुकता और जिज्ञासा को बनाए रखते हैं। मानव जीवन में आम और खास हर किसी को अनुभव में आने वाले पीड़ा और सुख, निराशा और आशा, लोभ और मोह, भय और साहस, हास-परिहास तथा प्रेम और घृणा जैसी भावनाओं के आरोह-अवरोह के अनेकानेक क्षण एक के बाद एक लगातार श्रीराम के जीवन में आते ही रहते हैं। वे मानों यही कहते लगते हैं कि यही मानव स्वभाव है और इसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है।
श्रीराम जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं वह अधर्म को हटा कर उसके स्थान पर धर्म की प्रतिष्ठा करने का एक युगांतरकारी अवसर है। सृष्टि बहुआयामी है और उसके सभी अवयव एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ये अवयव एक-दूसरे के साथ समरस रहते हैं तो अस्तित्व में जीवन का संचार करते हैं। दूसरी ओर जब किसी कारणवश उनके बीच असंतुलन खड़ा होता है तो विघ्न-बाधाएं आती हैं जिनका शमन होना ज़रूरी होता है। तभी व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो पाती है। इस तरह का परिवर्तन वाला क्रम सृष्टि के चक्रीय स्वभाव की अनिवार्य अपेक्षा है। श्रीराम को इसीलिए धर्म का विग्रह कहा गया (रामो विग्रहवान् धर्म:) कि वे सतत धर्म की स्थापना में जुटे रहते हैं। उनके होते अधर्म संभव नहीं है। इस रूप में वे उस विशाल भारतीय जन समाज की आत्मीयता के सुदृढ़ आधार हैं जिसमें अमीर, गरीब और पढ़े-लिखे से लेकर अनपढ़ तक सभी शामिल हैं।
यही कारण है कि आज भी लोग रामनवमी की तिथि पर श्रीराम के अवतरण की राह तकते हैं कि नाया विहान हो। धरती पर श्रीराम के प्रकट होने के क्षण की अनुभूति लोक के जीवन और स्मृति दोनों का एक सहज हिस्सा बनी हुई है। हो भी क्यों न ? राम की कथा आज भी आम आदमी की जिंदगी में घुली हुई है। श्रीराम सबके जाने पहचाने हैं। राम नाम का संकीर्तन स्वाभाविक रूप से बहुतों की जीवन-चर्या का अभिन्न अंग बना हुआ है। सुख हो या दुख, हर्ष हो या विषाद हर तरह के अवसर पर साँवले-सलोने, रघुवंशी, आजानबाहु, धनुषधारी श्रीराम को याद करते हुए लोक-जीवन का पहिया घूमता है। जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, शादी, ब्याह सभी संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों के नायक श्रीराम ही होते हैं। भक्ति मार्ग में उनकी महिमा लोक विश्रुत है। दीनदयाल श्रीराम भक्तों के संरक्षण के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सदैव उपलब्ध रहते हैं। निर्बल के बल तो राम ही होते हैं। ऐसा करते हुए श्रीराम जाति वर्ग नहीं वास्तविक भक्ति और प्रेम को महत्व देते हैं। वे जहाँ सबके प्रति उन्मुक्त भाव से उदार रहते हैं स्वयं अपने से निर्लिप्त बने रहते हैं। राज-भवन हो या जंगल सर्वत्र हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि श्रीराम अपरिवर्तित और अविचल ही बने रहते हैं। उनकी मानुषी लीला की कथा को देखें तो यही लगता है उनको लक्षित कर मिथ्यारोपों की सदैव झड़ी-सी लगी रहती है। सतत संघर्ष के बीच बचपन से ही पग-पग पर उनकी परीक्षा होती रहती है।
श्रीराम का आदर्श चरित इस अर्थ में विलक्षण है कि उसमें स्वयं अपने उदाहरणों द्वारा ही मर्यादाओं की व्यावहारिक स्तर पर व्याख्या की जाती है। विधि और निषेध अर्थात् क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका स्पष्टीकरण कराते हुए मर्यादाएँ जीवन में संतुलन स्थापित करती हैं। यह कुछ वैसे ही है जैसे नदी के दो तट यह बताते हैं कि नदी की धारा कैसे मर्यादा का आदर करते हुए एक सीमा में ही बहे। नदी में बाढ़ आने पर उफनती नदी के निकट का सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और आसपास की फसल और जन जीवन को भी भारी नुकसान पहुंचता है। वैसे ही मर्यादाओं का उल्लंघन भी सामाजिक जीवन के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। जब मर्यादाओं की सीमाएँ टूटती हैं तो सामान्य जन जीवन प्रतिबंधित और अस्त-व्यस्त हो जाता है। चूँकि सामान्य लोग श्रेष्ठ जनों या बड़ों का अनुगमन करते हैं इसलिए उच्च पदस्थ लोगों का यह दायित्व होता है कि वे न केवल मर्यादा का पालन करें बल्कि आवश्यकतानुसार नई मर्यादाओं को भी स्थापित करें। अतएव मर्यादा का हनन श्रीराम को किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए वे कोई भी कष्ट उठाने के लिए और अपने किसी भी हित का त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। अपने प्रिय जनों का साहचर्य सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा काम्य होता है। श्रीराम हैं कि राजपाट ही नहीं अपितु पूज्य पिता और परम प्रिय पत्नी दोनों का साहचर्य उन्हें खोना पड़ता है। उनको कई अवसरों पर दारुण वियोग सहन करना पड़ा। इन सब परिस्थितियों में वे अविचलित बने रहे और अपने कार्य और दायित्व के निर्वाह से कभी भी विमुख नहीं हुए।
मर्यादा सदैव पारस्परिक होती है और उसकी एक प्रमुख भूमिका समाज को बाँध कर सहेजने या कहें सुगठित और संगठित रखने की भी होती है। देश यह अनुभव कर रहा है कि मर्यादा के अभाव में कोई संगठन, विधानसभा या संसद सार्थक और सक्षम रूप से कार्य नहीं कर पाता है जिसका ख़ामियाज़ा सबको भोगना पड़ता है। इसी प्रकार विभिन्न पदों से जुड़ी भूमिकाओं का पद की गरिमा के अनुसार समुचित निर्वहन भी आवश्यक है। आज स्वार्थ, मोह और छल-कपट का बाज़ार गर्म है। नीति-अनीति, सत्य-असत्य और न्याय–अन्याय आदि का कोई ध्यान रखे बग़ैर उच्च पदस्थ लोग भी विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट आचरणों में लिप्त हो रहे हैं। यह दुखद है कि राजनीति, न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आए दिन आचरण की दृष्टि से कलुषित व्यवहार और मिथ्याचार की घटनाएँ अख़बारों में लगातार सुर्ख़ियाँ बन रही हैं। इसी के साथ अपराधों की दुनिया का तेज़ी से विस्तार हो रहा है।
ऐसे विकट हो रहे सामाजिक परिवेश में राम की प्रतीति और अनुभूति मार्गदर्शक भी है और आश्वस्त भी करने वाली है। आज हमें अपने भीतर के राम को जगाने की और राममय होने की आवश्यकता है। श्रीराम तो सभी गुणों के आगार हैं। श्रीराम का स्मरण और उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा मनुष्य को कुमार्गगामी होने से बचने और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उनकी तरह होने की कल्पना और उस दिशा में कदम बढ़ाते उनके पास चलना हर तरह से सुखदायक है। आज भी सत्य, धैर्य, धर्म, करुणा, क्षमा, मैत्री और अहिंसा आदि के पालन से ही जीवन को मूल्यवान बनाना संभव है। इसी पथ पर आगे बढ़ने में मानव का कल्याण निहित है। राम-राज्य का आशय दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों से मानव समाज की मुक्ति है। इसके लिए मन, बुद्धि और कर्म तीनों को पवित्र करना होगा। तभी विचार में बल आ सकेगा, मन स्फूर्ति का संचार होगा और हमारे कर्म फलवान हो सकेंगे। इसी वृत्ति के साथ सन्नद्ध होने पर ही देश के उत्थान के कार्य में कामयाबी मिल सकेगी।
गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में हम सब मूलतः ‘ईश्वर अंश जीव अविनाशी’ हैं पर हम अपना स्वभाव भूले रहते हैं। इस स्वरूप की अनदेखी कर अपनी सीमित अस्मिता के प्रलोभन में भटकते रहते हैं। हमें घट-घट में रमने वाले सर्वव्यापी राम को जगाना होगा। उन्हें जीवन में उतारने के लिए अपनी मर्यादाओं को अंगीकार करना होगा। मनुष्य जीवन का महत्व यही है कि उसमें यह विवेक शक्ति है कि वह अपने अस्तित्व के मूल प्रयोजन को पहचान सकता है, नई संभावनाओं को उद्घाटित कर सकता है।
(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश