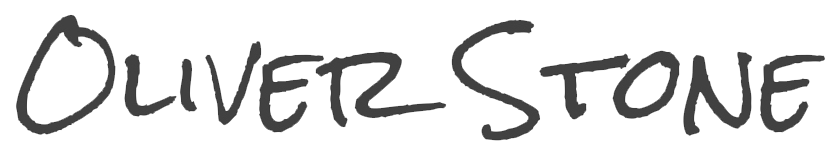Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
सामाजिक ताने-बाने में बदलाव को इस तरह से आसानी से समझा जा सकता है कि सोशियोट्रॉपी आज बीते जमाने की बात होती जा रही है। कोरोना के बाद तो हालात में और भी अधिक बदलाव आया है। आज की पीढ़ी में सामाजिकता का स्थान वैयक्तिकता लेती जा रही है। एक समय था जब सामाजिकता को वैयक्तिकता के स्थान पर अधिक तरजीह दी जाती थी। परिवार, मोहल्लों और आसपास कोई ना कोई ऐसे अवश्य मिल जाते थे जो जगत मामा तो कोई जगत काका तो कोई जगत दादा होते थे। छोटा हो या बड़ा, दादी हो या पोती, सास हो या बहू सब उन्हें प्रसिद्ध नाम से ही पुकारते थे। यह था एक तरह का अपनत्व। इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सभी के चहेते होते थे तो जान-पहचान हो या ना हो, वे जरूरत के समय पहुंच जाते थे। सुख-दुख खासतौर से मुसीबत के समय ऐसे व्यक्ति आगे रहते थे। हालांकि आज इस तरह के व्यक्तित्व को ढूंढ़ना लगभग असंभव सा है।
दरअसल, हमारी परंपरा व्यष्टि का ना होकर समष्टि की रही है। बच्चों को पहले सामाजिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। बच्चे मोहल्ले के सभी घरों को अपना ही घर मानकर चलते थे तो मोहल्ले में रहने वाले किसी का भी बच्चा हो उसे अपने बच्चे जितना ही प्यार और दुलार देते थे। दुख-दर्द में पूरा मोहल्ला साथ हो जाता था। मोहल्ले में किसी घर में मौत हो जाती थी तो पड़ोसी उस परिवार को संभालने और देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथ में ले लेते थे। शादी-विवाह में काम बंट जाता था, आज तो कैटरिंग का जमाना आ गया नहीं तो सैकड़ों लोगों को परिवार और मोहल्ले के युवा ही भोजन कराने की जिम्मेदारी निभा लेते थे। हलवाई के काम शुरू करते ही मोहल्ले के लोग बारी-बारी से देखरेख व सहयोग के लिए तैयार रहते थे। आज यह सब बदल गया है। गगनचुंबी इमारतों में कई परिवार रहते हैं और हालात यहां तक हो गए हैं कि एक ही कॉम्पलेक्स या अपार्टमेंट में रहने वाले एक-दूसरे को पहचानते नहीं। ऐसे में आपसी सहयोग और मेल-मिलाप की बात करना बेमानी होगा।
सोशियोट्रापी मनोविज्ञान में प्रयोग होता है। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थाें में लिया जाता है। दूसरों को खुश रखने की खुशी में अपने खुशी को भूल जाना वाली मनोस्थिति को भी सोशियोट्रापी के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि इस एकांगिग अर्थ को लेने के चक्कर में सोशियोट्रोपी मानसिकता वाले लोगों के अवसादग्रस्त, तनाव पीड़ित और हमेशा चिंतित रहने की मनोदशा को साइड इफेक्ट के रूप में देखा जाता है। जबकि सोशियोट्रापी यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरे के दुख-दर्द में भागीदार होना, आवश्यकता के समय निःस्वार्थ सहयोग व सहायता करना, दूसरे की परेशानी को समझना और उसे दूर करने में यथासंभव सहयोग करना यह सोशियोट्रापी का ही एक रूप है। हमारी परंपरा में जो व्यक्ति केवल अपने आप के बारे में सोचता है उसे एकलखोर या स्वार्थी कहा जाता रहा है। हमारी परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम की रही है। हमारी परंपरा में दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होने की भावना रही है। खुशी के मौके पर मिठाई बांटना खुशी में सभी को भागीदार बनाना है। इसी तरह से जरूरत के समय खड़े हो जाना जरूरतमंद के लिए संबल होता है।
देखा जाए तो बदलते सामाजिक ताना-बाना से सबकुछ बदल कर रख दिया है। एकल परिवार की संस्कृति समाज में अपना प्रभुत्व जमा चुकी है। परिवार पति-पत्नी और बच्चों तक सीमित होता जा रहा है। जो भावनात्मकता संबंधों को तरोताजा रखती थी वह भावनात्मकता कहीं खो गई है। अवकाश के दिनों का उपयोग दादा-दादी या नाना-नानी के पास गुजारने के स्थान पर कहीं घूमने में जाया होने लगा है। एक समय था जब गांव से यात्रा पर भी जाते थे तो गांव के कई परिवार के लोग उस भ्रमण दल में होते थे। हालात तो यहां तक होने लगे हैं कि घर के बुजुर्ग सदस्य को जिसे साथ की अधिक आवश्यकता है, घर की देखभाल के लिए छोड़ना आज आम होता जा रहा है। खुशी के पल को साझा करने का तरीका भी बदल गया है। जिस तरह की प्राथमिकताएं बदली हैं वह पीपल प्लीजर के स्थान पर सेल्फ प्लेजर होती जा रही है।
दरअसल सामाजिकता के जो मायने एक समय होते थे उसमें कोई क्या कहेगा महत्वपूर्ण होता था, सामाजिक प्रतिक्रिया का बड़ा भय होता था, आज हालात यह है कि मां-बाप क्या कहेंगे इसकी भी परवाह नहीं रही है। दरअसल न्यूक्लियर फैमेली के यह साइड इफैक्ट है जो लोगों को सोशियोट्रापी से दूर ले जाते हैं। पाश्चात्य देशों द्वारा अब इसकी अहमियत सामने आने लगी है। ब्रिटेन में पिछले दिनों एक अध्ययन में सामने आया है कि अब बच्चों का जब भी मौका मिलता है परिवार यानी दादा-दादी या नाना-नानी का साथ जरूरी माना जाने लगा है। क्योंकि सामाजिक ताना-बाना में बिखराव के कारण ही आज की पीढ़ी रिश्तों की अहमियत भूलती जा रही है। दादा-दादी या नाना-नानी में से एक तो पराया होता जा रहा है। जब खास रिश्तों के ही यह हालात होते जा रहे हैं, परिवार के मायने ही बदलते जा रहे हैं तो फिर अड़ोस-पड़ोस, मोहल्ले या शहर-गांव के रिश्तों की बात करना ही बेमानी होगा।
आज की पीढ़ी के सामाजिकता से दूर होने के नकारात्मक प्रभाव समाज के सामने आने लगे हैं। पाश्चात्य देश अब रिश्तों की अहमियत को समझने की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं वहीं हम रिश्तों की अहमियत और सामाजिकता खोते जा रहे हैं। यह अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। समाज और समाज विज्ञानियों व मनो विज्ञानियों को हालात की गंभीरता को समझते हुए समय रहते हालात को सुधारने के प्रयास करने होंगे।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश