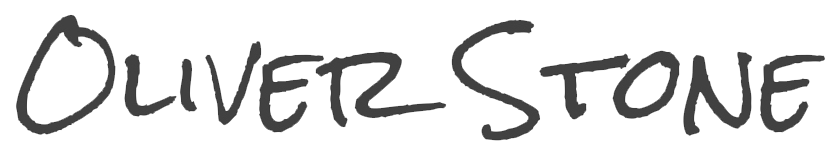Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

गिरीश्वर मिश्र
विधानसभा या लोकसभा के चुनाव राजनैतिक दलों के आंतरिक स्वभाव को उभार कर सामने लाने में बड़े मददगार होते हैं। दल कोई भी हो सत्ता हासिल करना और सत्तासीन होकर उस पर कब्जा बनाए रखना ही उनका परम धर्म हो चुका है। सत्ता के लिए आर्त पुकार जनता तक पहुँचाने की राजनीति जटिल और बहु आयामी होती जा रही है। चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक गहमागहमी तेज हो जाती है। नेताओं की अंतरात्मा जाग उठती है और सत्ता-यात्रा में आने वाले सारे बंधनों और अवरोधों को पार करने को छटपटाने लगती है। सत्ता के लिए वे किसी से कोई भी समझौता करने को व्यग्र दिखते हैं। वे अपना दल छोड़ कर दूसरे धुर विरोधी दल में प्रवेश लेने से नहीं कतराते। आज लगभग सभी दल इस तरह की उठापटक को जायज और स्वाभाविक ठहराते हैं, आख़िर युद्ध में सब कुछ उचित जो ठहरा।
चूँकि यह प्रवृत्ति किसी एक दल की न होकर सभी दलों की होती जा रही है, राजनैतिक हलकों में इसे सामान्य रणनीति का हिस्सा मान लिया जाता है। अब वैचारिक रुझान या किसी आदर्श या मूल्य से जुड़े आधार से ज़्यादातर दल अपना कोई रिश्ता नहीं रखते। सभी दलों के स्वर और रीति-नीति में बहुत अंतर नहीं दिखता। कभी राजा जी, मालवीय जी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य जेबी कृपालानी और डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे अनेक राजनेता वैचारिक और नीतिगत असहमति और जन-कल्याण के प्रश्नों पर टकराहट से अपनी मूल पार्टी से अलग हुए थे। अपनी दृष्टि के प्रति उनकी आस्था के पीछे कोई सीमित स्वार्थ नहीं था और वे उसके प्रति स्वाभाविक रूप से जुड़े थे। शायद वे उस जमाने के थे जब नि:स्वार्थ भाव से देश की सेवा और समाज के हित की दृष्टि से प्रेरित हो कर लोग राजनीति की ओर आते थे। इस सिलसिले में बहुतों ने पाने की जगह कुछ खोया गँवाया। राजनीति की दिशा में उनका कदम किसी निजी, पारिवारिक या समुदाय के दबाव से या दबदबा बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी पसंद से उठाया गया कदम होता था। उनकी नज़र समाज की कमियों और कमज़ोरियों का सामना करने पर रहती थी। ऐसे नेताओं की अच्छी संख्या होती थी जो अपने बलिदान और त्याग के लिए तैयार रहते थे। समाज की सेवा करने को उन्होंने चुना था।
राजनैतिक दलों की अपनी-अपनी वैचारिक पसंद नापसन्द तो होती थी और होनी भी चाहिए पर सबकुछ के बावजूद उन नेताओं के पास देश का एक नक़्शा होता था और बिना किसी संदेह के देशहित ही उनका सबसे महत्वपूर्ण सरोकार होता था। जमीन से उठ कर आने वाले ऐसे प्रामाणिक नेतृत्व की साख उनके द्वारा अर्जित होती थी। वे किसी हाईकमान की कृपा का मुंहताज नहीं होती थी। आज की तरह अपने लिए धनसंग्रह करते रहना उनका उद्देश्य नहीं होता था। उनमें देश-निर्माण का स्वाभाविक जज़्बा और उत्साह होता था जो उनके कार्यों में भी झलकता था। अब स्वतंत्र होने के पचहत्तर साल बीतने के बाद राजनैतिक परिवेश में जोड़-तोड़ की जो प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आ रही हैं वे राजनीति के तेजी से बदलते स्वभाव का संकेत दे रही हैं।
हर चुनाव की सुगबगाहट के साथ राजनैतिक दलों द्वारा रेवड़ी बाँटने की नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। वादों और घोषणाओं की झड़ी लग जा रही है। इसमें क्या कुछ नहीं शामिल होता है: नौकरी, बिजली, घर, सम्मान निधि, गैस सिलेंडर, कर्जमाफ़ी, सस्ता-कर्ज़, मुफ़्त वाई-फ़ाई, गरीब को वजीफ़े, आरक्षण की सुविधा यानी जो भी मन करे नेता लोग सब कुछ मतदाता को देने की घोषणा करते नहीं अघा रहे है। अब ज़मींदारों के तर्ज़ पर नेताजी मनमर्ज़ी से कोई भी एलान कर सकते हैं। मुफ़्त की सुविधायें देने के पीछे कोई आर्थिक-सामाजिक नीतिगत आधार नहीं होता है। जाति, उपजाति, क्षेत्र और धर्म जैसे आधार में बांध कर चुनाव की तैयारी कस्टमाइज्ड प्रलोभन देने की मुहिम चल रही है। इस तरह की प्रक्रिया का कोई ओर-छोर नहीं दिखाई पड़ता है। सुविधा और धन बाँट-बाँट कर जनता से वोट बटोरने की रीति-राजनीति में जन-भागीदारी को दूषित कर रही है। आज एमएलए और एमपी के चुनाव में करोड़ों के खर्च होते हैं। इसलिए प्रत्याशी भी करोड़पति होते हैं। ऊपर से संदिग्ध अपराधी भी शामिल होते हैं। अब धनबल और बाहुबल के बिना राजनीति की कल्पना कठिन हो रही है।
तुष्टिकरण के सहारे राजनीति लम्बी पारी नहीं खेल सकेगी। उल्टे यह देश की जड़ों को खोखला करने वाली युक्ति है। निर्वाचन आयोग, सरकार और राजनैतिक दलों को इसे नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम उठाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।
(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश